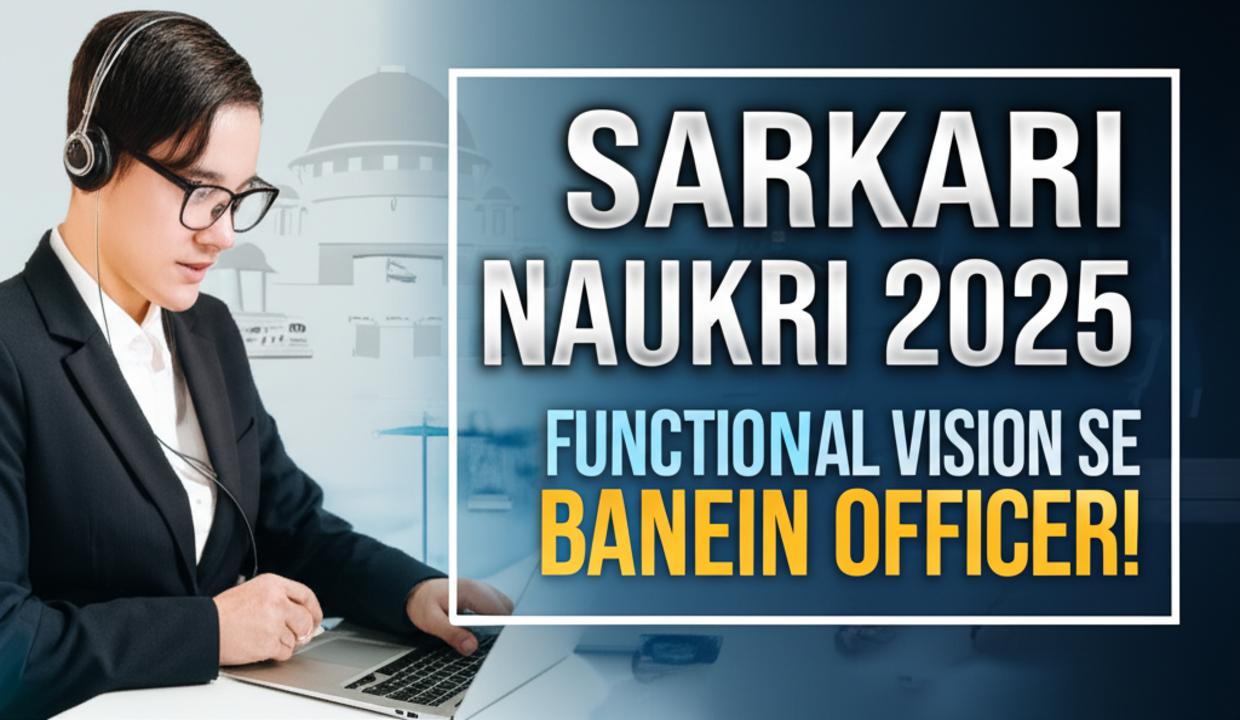नमस्कार! बहराइच न्यूज़ केऑटोमोबाइल सेक्शन में आपका स्वागत है।
आज के डिजिटल युग में, स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह सिर्फ एक संचार उपकरण नहीं, बल्कि ज्ञान, मनोरंजन और सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। पल-पल की खबरें हों या नवीनतम गैजेट्स की जानकारी, स्मार्टफोन हमें हर चीज़ से जोड़े रखता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर लाखों लोगों के भविष्य और सरकारी नौकरी के अवसरों को प्रभावित करती है। यह खबर एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी है, जो दिव्यांगजन रोजगार के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकती है, और यह स्मार्टफोन की तरह ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समावेशी समाज के निर्माण में एक बड़ा कदम है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक बड़े निर्णय की, जिसने कार्यात्मक दृष्टि की अवधारणा को मान्यता दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की मुख्य बातें
यह फैसला उन लोगों के लिए आशा की नई किरण लेकर आया है, जो अपनी शारीरिक सीमाओं के कारण अब तक अवसरों से वंचित थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए केवल शारीरिक दृष्टि ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यदि कोई उम्मीदवार सहायक उपकरणों या संज्ञानात्मक तरीकों से आवश्यक जानकारी को समझ सकता है, तो उसे ‘कार्यात्मक दृष्टि’ वाला माना जाएगा।
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| फैसले का विषय | सरकारी नौकरी के लिए ‘कार्यात्मक दृष्टि‘ की मान्यता। |
| अदालत का मत | शारीरिक दृष्टि आवश्यक नहीं; सहायक उपकरणों या संज्ञानात्मक तरीकों से जानकारी समझने की क्षमता पर्याप्त है। |
| ‘देखने’ की नई परिभाषा | यह सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्रिया से भी जुड़ा है। |
| प्रमुख कीवर्ड | सरकारी नौकरी, कार्यात्मक दृष्टि, दिल्ली हाई कोर्ट, दिव्यांगजन रोजगार। |
| प्रभाव | दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी 2025 और उसके बाद में रोजगार के अधिक अवसर खुलेंगे। |
| आधारभूत अधिनियम | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD एक्ट) के सिद्धांतों के अनुरूप। |
दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: ‘कार्यात्मक दृष्टि’ को मिली पहचान
हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसने देश में सरकारी नौकरी के परिदृश्य को बदल दिया है। अदालत ने फैसला दिया है कि नौकरी के कार्यों को पूरा करने के लिए केवल “शारीरिक दृष्टि” ही अनिवार्य नहीं है। यदि कोई उम्मीदवार सहायक उपकरणों या अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करके आवश्यक जानकारी को प्रभावी ढंग से समझ सकता है, तो उसे उस पद के लिए उपयुक्त माना जाएगा। यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि “देखना” केवल आंखों की शारीरिक क्रिया से कहीं अधिक है; यह मस्तिष्क की संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली से जुड़ा है, जो जानकारी को संसाधित करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय उन तीन नेत्रहीन उम्मीदवारों की याचिका के आंशिक पक्ष में आया है, जिन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) में जूनियर इंजीनियर (लॉ) के पदों के लिए अस्वीकृत कर दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई नेत्रहीन उम्मीदवार, सहायक उपकरणों की मदद से, नौकरी के कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है, तो उसके पास सरकारी नौकरी के लिए पर्याप्त कार्यात्मक दृष्टि है। यह फैसला समावेशी समाज की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो व्यक्तियों की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि उनकी सीमाओं पर।
‘कार्यात्मक दृष्टि’ की विस्तृत व्याख्या
कार्यात्मक दृष्टि एक ऐसी अवधारणा है जो पारंपरिक दृष्टि से कहीं आगे जाती है। यह किसी व्यक्ति की वैकल्पिक माध्यमों से नौकरी के आवश्यक कार्यों को करने की क्षमता को संदर्भित करती है, खासकर जब शारीरिक दृष्टि कमजोर हो। इसमें सहायक तकनीक का उपयोग, स्पर्श-संवेदी विधियां, श्रवण संकेत, या केवल संज्ञानात्मक समझ शामिल हो सकती है। अदालत ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से यह स्पष्ट किया कि आंखें केवल जानकारी को रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने का काम करती हैं, लेकिन जानकारी को समझने और संसाधित करने का वास्तविक कार्य मस्तिष्क में होता है। इसलिए, दृश्य हानि स्वचालित रूप से उम्मीदवारों को अयोग्य नहीं ठहराती है, बशर्ते कार्यात्मक आवश्यकताएं अन्य सहायक उपकरणों या संज्ञानात्मक कौशल द्वारा पूरी की जा सकें। यह नई अवधारणा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD) के समावेशिता के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। इसका उद्देश्य दृश्य हानि या अंधत्व से पीड़ित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है। उदाहरण के लिए, एक नेत्रहीन व्यक्ति स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कंप्यूटर पर दस्तावेज़ पढ़ सकता है, या ब्रेल डिस्प्ले की मदद से डेटा का विश्लेषण कर सकता है। ये सभी कार्य उसकी कार्यात्मक दृष्टि का ही हिस्सा हैं। इस तरह के समावेशी दृष्टिकोण से सरकारी नौकरी में दिव्यांगजन रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में अवसर: RPwD एक्ट की भूमिका
भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्रों में कुछ पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, जिनमें नेत्रहीनता या कम दृष्टि वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, श्रेणी A, B, C और D में 1% पद नेत्रहीनता या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। यह आरक्षण नीति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा निर्धारित की जाती है, जो दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती है। DoPT और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आरक्षण नीतियों और कौशल वर्गीकरण प्रणालियों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में उपयुक्त भूमिकाएं खोजने में मदद करते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। RPwD अधिनियम, 2016, दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत, सभी सरकारी प्रतिष्ठानों को एक ‘समान अवसर नीति’ (EOP) बनानी अनिवार्य है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के प्रावधान शामिल हों।
समान अवसर नीति (EOP) का महत्व
समान अवसर नीति (EOP) उन कंपनियों के लिए अनिवार्य है जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी हैं। यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग व्यक्तियों को भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन और पदोन्नति में समान अवसर मिलें। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि सुलभ बुनियादी ढांचा (जैसे रैंप, लिफ्ट), सहायक उपकरण (जैसे स्क्रीन रीडर, ब्रेल कीबोर्ड), आवास और शिकायत निवारण के लिए संपर्क अधिकारी, और उपयुक्त पदों की पहचान। उदाहरण के लिए, एक बड़ी सरकारी कंपनी में, EOP यह सुनिश्चित करेगी कि एक व्हीलचेयर उपयोगकर्ता के लिए कार्यालय में आवागमन सुगम हो, और एक श्रवण बाधित कर्मचारी को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की सुविधा मिले। एक नेत्रहीन व्यक्ति जिसे डेटा एंट्री या कानूनी अनुसंधान का काम दिया गया है, उसे आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसे स्क्रीन रीडर या वॉयस रिकॉग्निशन टूल उपलब्ध कराए जाएंगे। यह उसे अपने कार्य को कुशलता से करने में सक्षम बनाएगा, जिससे उसकी शारीरिक सीमाएं उसके काम में बाधा नहीं बनेंगी। यह EOP सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिबद्धता है कि कार्यस्थल पर हर व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के आधार पर महत्व दिया जाए। यह दिव्यांगजन रोजगार को एक नई दिशा देती है, जिससे वे सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सकें।
रोजगार वर्गीकरण और मूल्यांकन मानक
सरकारी नौकरी में दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त भूमिकाएं खोजने और भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, रोजगार वर्गीकरण और मूल्यांकन मानकों का उपयोग किया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय व्यावसायिक वर्गीकरण (NCO 2015) का उपयोग नौकरियों को वर्गीकृत करने और दिव्यांग व्यक्तियों को उपयुक्त भूमिकाओं के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि सही व्यक्ति को सही नौकरी मिले, और उनकी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। यह डेटा प्रसंस्करण को भी सुव्यवस्थित करता है और रोजगार के आंकड़ों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इसके अलावा, अमेरिका में, कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (Office of Personnel Management) का व्यावसायिक समूह और परिवार का हैंडबुक (Handbook of Occupational Groups and Families) व्यावसायिक आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए “कार्यात्मक मानकों” को परिभाषित करता है। यह शारीरिक क्षमताओं के बजाय नौकरियों में कार्यात्मक क्षमता की भूमिका पर जोर देता है। भारत में भी, इस तरह के मानक दिव्यांगजनों को उनकी विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर विभिन्न पदों के लिए मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया समावेशी और न्यायसंगत हो, और उम्मीदवारों को केवल उनकी शारीरिक सीमाओं के आधार पर खारिज न किया जाए। इन मानकों के माध्यम से, सरकारी नौकरी में दिव्यांगजन रोजगार के लिए अधिक स्पष्ट और निष्पक्ष प्रणाली स्थापित की जा सकती है।
तकनीकी प्रगति और बदलती न्यायिक सोच
दिल्ली हाई कोर्ट का हालिया फैसला न्यायपालिका और नीतिगत हलकों में दिव्यांगता की समावेशी पुनर्व्याख्या करने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह सिर्फ शारीरिक गुणों के बजाय क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, खासकर रोजगार के क्षेत्र में। यह एक सकारात्मक बदलाव है जो समाज में दिव्यांगजनों की भागीदारी को मजबूत करेगा। सहायक प्रौद्योगिकियों, जैसे कि स्क्रीन रीडर, ब्रेल डिस्प्ले, ऑडियो आउटपुट और आवाज पहचान का बढ़ता उपयोग, नौकरी तक पहुंच को और बढ़ा रहा है। ये उपकरण दिव्यांग व्यक्तियों को उन कार्यों को करने में सक्षम बनाते हैं जो पहले उनके लिए दुर्गम लगते थे। उदाहरण के लिए, एक वकील जो नेत्रहीन है, वह अब स्क्रीन रीडर की मदद से कानूनी दस्तावेजों को पढ़कर, अपनी सुनवाई में तर्क प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार, एक सरकारी कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति वॉयस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नोट्स ले सकता है या ईमेल लिख सकता है। भारत सरकार रोजगार प्रणालियों और करियर सेवाओं को आधुनिक बनाने में सक्रिय है, जैसे राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल, ताकि भर्ती पारदर्शिता में सुधार हो सके और रोजगार प्रक्रिया दिव्यांगता-अनुकूल बन सके। इन प्रयासों के बावजूद, दृश्य अक्षमता वाले व्यक्तियों को अभी भी नौकरी तक पहुंच में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो मजबूत प्रवर्तन और जागरूकता पहलों की आवश्यकता को इंगित करता है।
सहायक उपकरणों का बढ़ता प्रभाव
सहायक उपकरण जैसे स्क्रीन रीडर, ब्रेल डिस्प्ले, और वॉयस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ने दिव्यांगजन रोजगार के अवसरों को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। पहले, कई सरकारी नौकरी के पद नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए असंभव माने जाते थे। लेकिन अब, इन तकनीकों की मदद से, वे डेटा विश्लेषण, ग्राहक सेवा, कानूनी परामर्श और यहां तक कि कुछ इंजीनियरिंग भूमिकाएं भी निभा सकते हैं। एक नेत्रहीन व्यक्ति एक स्क्रीन रीडर का उपयोग करके जटिल स्प्रेडशीट का विश्लेषण कर सकता है, या वॉयस कमांड के माध्यम से सॉफ्टवेयर विकसित कर सकता है। ये उपकरण उन्हें सूचना तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने और उसे संसाधित करने की शक्ति देते हैं, जिससे उनकी कार्यात्मक दृष्टि सशक्त होती है। यह सिर्फ नौकरी पाने के बारे में नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर समान रूप से योगदान करने और अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के बारे में है। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में इन उपकरणों को अपनाना दिव्यांगजन रोजगार के लिए एक उज्जवल भविष्य का संकेत है।
भविष्य की राह: ‘कार्यात्मक दृष्टि’ आधारित रोजगार
दिल्ली हाई कोर्ट का यह ऐतिहासिक निर्णय अन्य सरकारी निकायों और निजी नियोक्ताओं के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। यह उन्हें दिव्यांगता मानदंडों का पुनर्मूल्यांकन करने और उन्हें कार्यात्मक क्षमता के आधार पर स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा। यह बदलाव सरकारी नौकरी 2025 और उसके बाद के वर्षों में दिव्यांगजन रोजगार के लिए नए द्वार खोलेगा। कार्यस्थलों में सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों को अपनाने और बेहतर विधायी उपायों से पहुंच में और सुधार हो सकता है। इसका मतलब है कि कार्यस्थल को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वह सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी शारीरिक क्षमता कुछ भी हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सहायक उपकरणों में तेजी से हो रहे तकनीकी नवाचारों से दृश्य बाधित व्यक्तियों के लिए विभिन्न सरकारी भूमिकाओं में रोजगार की संभावनाएं और भी व्यापक होने की उम्मीद है। AI-संचालित उपकरण अब पहले से कहीं अधिक परिष्कृत हो रहे हैं, जो जटिल कार्यों को सरल बना सकते हैं। आरक्षण नीतियों की निगरानी और कार्यात्मक मूल्यांकनों के साथ उनका तालमेल बिठाना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रभावी नौकरी प्लेसमेंट को बढ़ा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि नीतियां केवल कागज़ पर ही न रहें, बल्कि वास्तविक जीवन में भी लागू हों, जिससे सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सकें। इस फैसले से समाज में दिव्यांगजनों के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे वे भी देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के फायदे और संभावित चुनौतियां
| फायदे (Pros) | संभावित चुनौतियां (Cons) |
|---|---|
| समावेशी समाज: कार्यात्मक दृष्टि की मान्यता से दिव्यांगजनों के लिए अधिक समावेशी समाज का निर्माण होगा। | जागरूकता का अभाव: नियोक्ताओं और जनता के बीच कार्यात्मक दृष्टि की नई अवधारणा के बारे में जागरूकता बढ़ाना चुनौती होगी। |
| बढ़ते अवसर: सरकारी नौकरी 2025 में दिव्यांगजन रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। | बुनियादी ढांचे का विकास: सभी सरकारी कार्यालयों में सुलभ बुनियादी ढांचा और सहायक उपकरणों का प्रावधान करना एक बड़ी चुनौती होगी। |
| तकनीकी प्रोत्साहन: सहायक प्रौद्योगिकियों और AI के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कार्यस्थल अधिक सुलभ बनेंगे। | मूल्यांकन मानकों का अनुकूलन: कार्यात्मक दृष्टि के आधार पर नौकरी के लिए उम्मीदवारों का सही मूल्यांकन करने के लिए नए, स्पष्ट मानकों की आवश्यकता होगी। |
| आत्मनिर्भरता: दिव्यांगजन अपनी क्षमताओं के आधार पर आत्मनिर्भर बन सकेंगे और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकेंगे। | प्रतिरोध: कुछ संस्थानों या व्यक्तियों की ओर से बदलाव के प्रति शुरुआती प्रतिरोध या अनिच्छा का सामना करना पड़ सकता है। |
| कानूनी स्पष्टता: RPwD अधिनियम के तहत रोजगार प्रावधानों को और अधिक स्पष्टता मिलेगी, जिससे विवाद कम होंगे। | प्रशिक्षण की आवश्यकता: मूल्यांकनकर्ताओं और भर्ती अधिकारियों को नई मूल्यांकन प्रक्रियाओं और कार्यात्मक दृष्टि को समझने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी में कार्यात्मक दृष्टि को क्यों मान्यता दी है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी में कार्यात्मक दृष्टि को मान्यता इसलिए दी है, ताकि दिव्यांगजनों को उनकी क्षमताओं के आधार पर समान अवसर मिल सकें। अदालत का मानना है कि ‘देखना’ केवल शारीरिक आंखों तक सीमित नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमता से भी जुड़ा है। यह फैसला RPwD एक्ट के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य समावेशी समाज का निर्माण करना है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक सीमा के कारण अवसरों से वंचित न रहे।
Q2: कार्यात्मक दृष्टि का क्या अर्थ है और यह पारंपरिक दृष्टि से कैसे अलग है?
कार्यात्मक दृष्टि का अर्थ है सहायक उपकरणों (जैसे स्क्रीन रीडर, ब्रेल) या अन्य वैकल्पिक विधियों (जैसे श्रवण या स्पर्श) का उपयोग करके नौकरी के आवश्यक कार्यों को करने की क्षमता। यह पारंपरिक दृष्टि से इसलिए अलग है क्योंकि यह केवल आंखों की शारीरिक क्षमता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मस्तिष्क की जानकारी को संसाधित करने की क्षमता पर जोर देती है, भले ही जानकारी तक पहुंचने का तरीका कुछ भी हो।
Q3: इस फैसले से दिव्यांगजन रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस फैसले से दिव्यांगजन रोजगार के अवसरों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब अधिक दिव्यांगजन, विशेषकर नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह फैसला सरकारी नौकरी 2025 में समावेशिता को बढ़ाएगा, जिससे उन्हें उन पदों पर काम करने का मौका मिलेगा, जो पहले उनकी पहुंच से बाहर माने जाते थे। यह आत्मनिर्भरता और सम्मान को भी बढ़ावा देगा।
Q4: सहायक उपकरण दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी में कैसे मदद करते हैं?
सहायक उपकरण जैसे स्क्रीन रीडर, ब्रेल डिस्प्ले, और वॉयस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर दिव्यांगजनों को जानकारी तक पहुंचने, उसे समझने और कार्य करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, एक नेत्रहीन व्यक्ति स्क्रीन रीडर की मदद से कंप्यूटर पर दस्तावेज पढ़ सकता है या ईमेल लिख सकता है। ये उपकरण उनकी कार्यात्मक दृष्टि को सशक्त बनाते हैं, जिससे वे उन कार्यों को प्रभावी ढंग से कर पाते हैं, जिनके लिए पहले शारीरिक दृष्टि की आवश्यकता होती थी।
Q5: क्या यह फैसला निजी क्षेत्र की कंपनियों पर भी लागू होगा?
हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला सीधे तौर पर सरकारी नौकरी से संबंधित है, यह निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है। RPwD एक्ट, जिसके सिद्धांतों पर यह फैसला आधारित है, निजी कंपनियों को भी समान अवसर नीति (EOP) अपनाने का निर्देश देता है। इसलिए, उम्मीद है कि निजी क्षेत्र भी धीरे-धीरे कार्यात्मक दृष्टि की अवधारणा को अपनाएगा, जिससे दिव्यांगजन रोजगार के अवसर व्यापक होंगे।