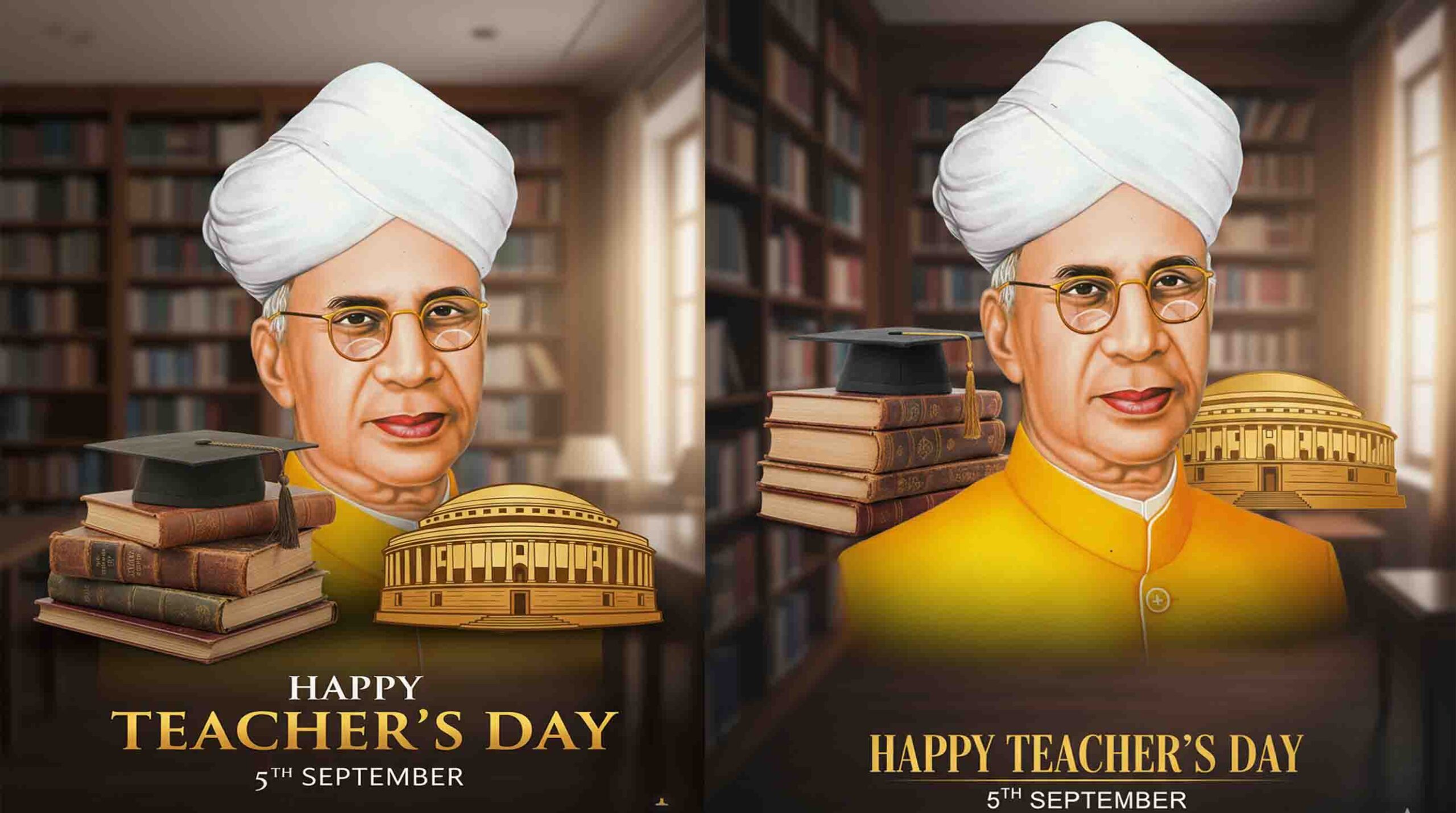नमस्कार! बहराइच न्यूज़ में आपका स्वागत है।
आज 5 सितंबर है, एक ऐसी तारीख जो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यह केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक प्रतीक है ज्ञान, सेवा और विनम्रता का। यह उस महापुरुष का जन्मदिन है जिन्होंने एक शिक्षक के साधारण जीवन से लेकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक की यात्रा की और दुनिया को भारतीय दर्शन की गहराई से परिचित कराया। हम बात कर रहे हैं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की।
आज शिक्षक दिवस के इस विशेष अवसर पर, बहराइच न्यूज़ आपको डॉ. राधाकृष्णन के जीवन के हर पहलू से परिचित कराएगा – उनके बचपन से लेकर उनके विचारों की दुनिया तक, और एक शिक्षक से ‘दार्शनिक राजा’ बनने तक के उनके असाधारण सफर की यह कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की नींव
किसी भी महान व्यक्तित्व की कहानी की जड़ें उसके बचपन और प्रारंभिक संघर्षों में छिपी होती हैं। डॉ. राधाकृष्णन का जीवन भी इसका अपवाद नहीं था। उनका आरंभिक जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उनकी असाधारण प्रतिभा और ज्ञान की प्यास ने उन्हें महानता के शिखर पर पहुँचाया।
तिरुत्तानी का एक साधारण बालक
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर, 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे तिरुत्तानी में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह स्थान आज के चेन्नई शहर से लगभग 64 किलोमीटर दूर है। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था; उनके पिता एक स्थानीय जमींदार के यहाँ एक साधारण राजस्व अधिकारी के रूप में काम करते थे।
उनके पिता की गहरी धार्मिक आस्था थी और उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहकर एक पुजारी बने। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बालक राधाकृष्णन के मन में ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी लौ जल रही थी, जिसे कोई रोक नहीं सका।
ज्ञान की ओर बढ़ते कदम
राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा तिरुत्तानी के के.वी. हाई स्कूल में हुई। इसके बाद 1896 में, वे तिरुपति के हर्मन्सबर्ग इवेंजेलिकल लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ने चले गए। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वेल्लोर के वूरहीस कॉलेज से पूरी की। वे बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे और अपनी पूरी शिक्षा के दौरान उन्हें छात्रवृत्तियाँ मिलती रहीं, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च चलता रहा।
उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने 17 साल की उम्र में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो उस समय के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक था। यहीं से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। दिलचस्प बात यह है कि दर्शनशास्त्र (Philosophy) उनका पहला पसंदीदा विषय नहीं था। आर्थिक तंगी के कारण, जब उनके एक चचेरे भाई ने उसी कॉलेज से दर्शनशास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी की, तो उन्होंने अपनी किताबें राधाकृष्णन को दे दीं। इन्हीं किताबों ने राधाकृष्णन को दर्शनशास्त्र की दुनिया से जोड़ा और उन्होंने इसी विषय में अपनी आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया।
“वेदांत का नीतिशास्त्र” – एक असाधारण शुरुआत
1906 में, मात्र 20 वर्ष की आयु में, उन्होंने दर्शनशास्त्र में मास्टर डिग्री (एम.ए.) पूरी की। उनकी एम.ए. की थीसिस का शीर्षक था “द एथिक्स ऑफ वेदांत एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रेसपोजिशन्स” (The Ethics of Vedanta and Its Metaphysical Presuppositions)। इस शोध-प्रबंध ने उनके प्रोफेसरों, रेव विलियम मेस्टन और डॉ. अल्फ्रेड जॉर्ज हॉग को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने राधाकृष्णन की दार्शनिक प्रतिभा को पहचाना और उनकी थीसिस को प्रकाशित करने की सिफारिश की। जब यह प्रकाशित हुई, तो इसने अकादमिक जगत में एक युवा दार्शनिक के आगमन की घोषणा कर दी।
एक शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में स्वर्णिम यात्रा
डॉ. राधाकृष्णन के हृदय में हमेशा एक शिक्षक बसता था। उनका मानना था कि सच्चा शिक्षक वह है जो छात्रों को केवल तथ्य नहीं रटाता, बल्कि उन्हें सोचना सिखाता है और उनके चरित्र का निर्माण करता है। उनका अकादमिक जीवन उनकी इसी सोच का प्रतिबिंब था।
विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन
अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, 1909 में, डॉ. राधाकृष्णन को मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज के दर्शनशास्त्र विभाग में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ से उनके शानदार अकादमिक करियर की शुरुआत हुई। 1918 में, वे मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1921 में, उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया। उनके व्याख्यान इतने ज्ञानवर्धक और आकर्षक होते थे कि छात्र दूसरी कक्षाओं से भी उन्हें सुनने के लिए आ जाते थे।
कुलपति का कार्यकाल और प्रशासनिक कौशल
अध्यापन के साथ-साथ, डॉ. राधाकृष्णन ने एक कुशल प्रशासक की भूमिका भी निभाई। उन्होंने 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया। 1939 में, पंडित मदन मोहन मालवीय के विशेष आग्रह पर, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के कुलपति का पदभार संभाला और 1948 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने इन विश्वविद्यालयों को अकादमिक उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ऑक्सफ़ोर्ड में भारतीय दर्शन की ध्वजा
उनकी ख्याति भारत की सीमाओं को पार कर चुकी थी। 1936 में, उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पैल्डिंग प्रोफेसर (Spalding Professor of Eastern Religions and Ethics) के रूप में नियुक्त किया गया। वे इस प्रतिष्ठित पद को धारण करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत की गहनता और तार्किकता से परिचित कराया। उन्होंने भारतीय विचारों को एक आधुनिक और सुलभ तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे पश्चिम में भारतीय दर्शन के प्रति सम्मान और समझ बढ़ी।
दार्शनिक राधाकृष्णन: पूर्व और पश्चिम के सेतु
डॉ. राधाकृष्णन 20वीं सदी के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। उनका मुख्य योगदान पूर्वी और पश्चिमी दर्शन के बीच एक सेतु का निर्माण करना था।
अद्वैत वेदांत के प्रखर प्रवक्ता
उनका दर्शन मुख्य रूप से अद्वैत वेदांत की परंपरा पर आधारित था, जो आत्मा (आत्मान) और परम सत्य (ब्रह्म) की एकता पर जोर देता है। उन्होंने शंकराचार्य के विचारों की एक समकालीन व्याख्या प्रस्तुत की। उनका मानना था कि आध्यात्मिकता केवल एक अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जिसे तर्क और अंतर्ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
भारतीय दर्शन की वैश्विक व्याख्या
उस समय कई पश्चिमी विद्वान हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन की आलोचना करते थे और उसे अतार्किक मानते थे। डॉ. राधाकृष्णन ने इन आलोचनाओं का दृढ़ता से खंडन किया। उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से यह साबित किया कि हिंदू धर्म एक गहरी तार्किक और वैज्ञानिक नींव पर आधारित है। उन्होंने पश्चिमी दर्शन और ईसाई धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया और तुलनात्मक धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ
डॉ. राधाकृष्णन एक विपुल लेखक थे। उन्होंने दर्शन और धर्म पर कई किताबें लिखीं, जो आज भी क्लासिक्स मानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में शामिल हैं:
- “इंडियन फिलॉसफी” (दो खंडों में): यह भारतीय दर्शन पर लिखी गई सबसे व्यापक और आधिकारिक पुस्तकों में से एक है।
- “द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स”: इसमें उन्होंने उपनिषदों के गहन संदेशों की व्याख्या की है।
- “एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ”: यह उनके प्रसिद्ध हिबर्ट लेक्चर्स का संग्रह है, जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड में दिए थे।
- “द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ”: इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया है।
राजनयिक और राजनेता: राष्ट्र सेवा का पथ
एक सफल शिक्षाविद और दार्शनिक होने के बाद, डॉ. राधाकृष्णन ने राष्ट्र की राजनीतिक सेवा में भी कदम रखा। उनका राजनीतिक जीवन भी उनके व्यक्तित्व की तरह ही गरिमापूर्ण और आदर्शवादी था।
सोवियत संघ में भारत के राजदूत
भारत की स्वतंत्रता के बाद, 1949 में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉ. राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत का विशेष राजदूत नियुक्त किया। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि उस समय सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन से मिलना लगभग असंभव था। लेकिन डॉ. राधाकृष्णन अपनी विद्वता और शांत व्यक्तित्व से स्टालिन को भी प्रभावित करने में सफल रहे।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति
1952 में, डॉ. राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से भारत का पहला उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने इस पद पर लगातार दो कार्यकालों (1952-1962) तक सेवा की। उपराष्ट्रपति के रूप में, वे राज्यसभा के सभापति भी थे। उन्होंने सदन की कार्यवाही को गरिमा और निष्पक्षता के साथ संचालित किया और स्वस्थ बहस के उच्च मानक स्थापित किए।
भारत के द्वितीय राष्ट्रपति: ‘दार्शनिक राजा’
1962 में, डॉ. राजेंद्र प्रसाद के बाद, वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति बनने पर, प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रेंड रसेल ने कहा था, “यह प्लेटो का सपना सच होने जैसा है कि एक दार्शनिक भारत का राष्ट्रपति बना है।” उनके कार्यकाल (1962-1967) के दौरान भारत ने दो युद्धों (1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ) का सामना किया, लेकिन उन्होंने देश का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और राष्ट्र का मनोबल बनाए रखा।
शिक्षक दिवस: एक अनूठी विरासत
डॉ. राधाकृष्णन की सबसे स्थायी विरासतों में से एक ‘शिक्षक दिवस’ की परंपरा है। जब वे 1962 में राष्ट्रपति बने, तो उनके कुछ छात्र और मित्र उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके पास पहुँचे। इस पर डॉ. राधाकृष्णन ने एक विनम्र अनुरोध किया। उन्होंने कहा, “मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय, यदि 5 सितंबर को ‘शिक्षक दिवस’ के रूप में मनाया जाए, तो यह मेरे लिए गौरवपूर्ण सौभाग्य होगा।”
उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए, 1962 से भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षकों के अमूल्य योगदान और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सम्मान, पुरस्कार और अंतिम वर्ष
डॉ. राधाकृष्णन को उनके जीवनकाल में अनगिनत सम्मान और पुरस्कार मिले, जो उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं।
पुरस्कारों की लंबी सूची
- नाइटहुड (1931): ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें ‘सर’ की उपाधि दी गई, हालांकि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने इसे त्याग दिया।
- भारत रत्न (1954): उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया।
- ऑर्डर ऑफ मेरिट (1963): ब्रिटिश क्राउन द्वारा दिया जाने वाला एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान।
- टेम्पलटन पुरस्कार (1975): धर्म और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया।
- नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन: उन्हें 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था (16 बार साहित्य के लिए और 11 बार शांति के लिए), जो उनकी अंतरराष्ट्रीय विद्वता का प्रमाण है।
जीवन का अंतिम अध्याय
राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद, वे चेन्नई में बस गए और अपना समय अध्ययन और लेखन में बिताया। 17 अप्रैल, 1975 को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
निष्कर्ष: एक प्रकाशस्तंभ जो आज भी प्रासंगिक है
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्था थे। वे एक महान शिक्षक, एक गहरे दार्शनिक, एक कुशल राजनयिक और एक आदर्शवादी राजनेता का अद्भुत संगम थे। उन्होंने साबित किया कि ज्ञान की शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से बड़ी है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन को विश्व मंच पर जो सम्मान दिलाया, वह अतुलनीय है।
उनका जीवन हमें सिखाता है कि विनम्रता, ज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलकर साधारण परिस्थितियों से उठकर भी असाधारण ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षक दिवस पर, हम इस महान गुरु को नमन करते हैं, जिनका जीवन और जिनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।